‘इंटरनेशनल खिलाड़ी’ बनने के लिए रुपये को करना होगा लंबा इंतजार, चीन जला चुका है अपने हाथ
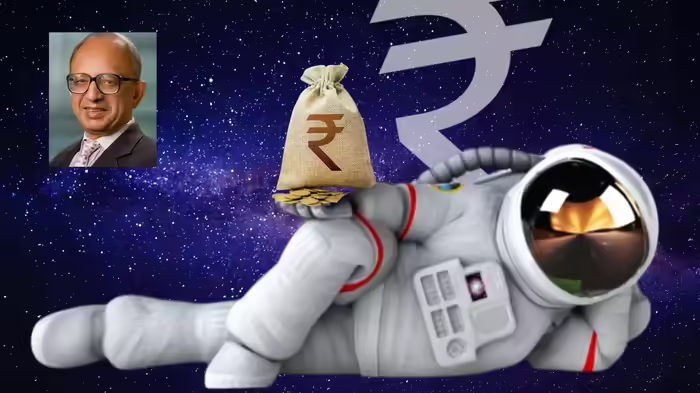
दुनिया के सभी देश अमेरिका की करेंसी डॉलर से ईर्ष्या रखते हैं। फाइनेंस और ट्रेड में डॉलर की धाक ऐसी है कि कोई भी देश इसे टक्कर नहीं दे पाता। ज्यादातर बड़े-बड़े व्यापार और निवेश के सौदे डॉलर में ही होते हैं, भले ही अमेरिका उस सौदे में शामिल न हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भी चाहता है कि भारतीय रुपया भी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी युआन (RMB) की तरह एक ‘रिजर्व करेंसी’ बन जाए। आम जनता को भी यह बात अच्छी लगती है।
पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपया को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए कुछ कदम उठाए। मीडिया ने इन कदमों का स्वागत किया। हालांकि, ये कदम बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि छोटे-छोटे थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हमें सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए। हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों का ध्यान रखना होगा।
डॉलर पर निर्भरता
इसका सीधा मतलब यह है कि भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इससे निर्यातकों का खर्च कम होगा और धीरे-धीरे रुपया को व्यापार और निवेश के लिए एक भरोसेमंद मुद्रा के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह कदम भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनने की चाहत के अनुरूप भी है
चीन का अनुभव
चीन का एक दशक पहले का अनुभव एक बड़ी चेतावनी है। चीन जैसी आर्थिक रूप से मजबूत और समझदार देश को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जैसे देश को भी अपनी पूंजी खाते को पूरी तरह से खुला बनाने में दशकों लग गए और इस दौरान उसे कई गंभीर संकटों से गुजरना पड़ा। 2010 के दशक की शुरुआत में चीन बहुत आत्मविश्वास से भरा था। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, उसका व्यापार घाटा बहुत कम था और उसके पास 4 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। एक महाशक्ति बनने की तैयारी में बीजिंग ने युआन (RMB) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना शुरू किया।
उनकी योजना बहुत बड़ी थी: युआन को व्यापार के बिलों और भुगतान में इस्तेमाल को बढ़ावा देना, हांगकांग और लंदन में ऑफशोर युआन बाजार बनाना और सीमित मात्रा में पूंजी को बाहर जाने की अनुमति देना। 2014 के अंत तक चीन के लगभग एक चौथाई व्यापार का भुगतान युआन में होने लगा था और युआन को IMF की स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDR) बास्केट में भी शामिल कर लिया गया था, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर असली परीक्षा का समय आया।
2015 में लाखों चीनी नागरिक युआन की संपत्तियों से निकलकर डॉलर की संपत्तियों में निवेश करने लगे। युआन की कीमत तेजी से गिरने लगी। कमजोरी को भांपते हुए, घरेलू और विदेशी निवेशकों ने देश से पैसा निकालना शुरू कर दिया। पूंजी का पलायन बहुत बढ़ गया और चीन ने 1 ट्रिलियन डॉलर का अपना विदेशी मुद्रा भंडार खो दिया।
बीजिंग ने फिर से सख्त पूंजी नियंत्रण लागू कर दिए। एक मजबूत मुद्रा बनने की महत्वाकांक्षी कोशिश एक शर्मनाक हार में बदल गई। इससे एक कड़वा सबक मिला: एक विशाल अर्थव्यवस्था भी, जिसके पास गहरा भंडार हो, एक साथ पूंजी प्रवाह को खुला नहीं रख सकती, अपनी विनिमय दर को नियंत्रित नहीं कर सकती और अपनी मौद्रिक स्वायत्तता को पूरी तरह से बनाए नहीं रख सकती। भारत के लिएयह जोखिम कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि उसके पूंजी बाजार और भी छोटे हैं और विदेशी मुद्रा भंडार कम है।
ब्रिटेन का मामला
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का इतिहास दिखाता है कि कैसे 19वीं सदी की दुनिया की वित्तीय महाशक्ति आधुनिक पूंजी बाजारों के कारण कमजोर पड़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी अंतरराष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह रुक गया था। अमेरिका ने मार्शल सहायता और अन्य ऋण समझौतों के तहत ब्रिटेन को स्टर्लिंग को फिर से परिवर्तनीय बनाने के लिए मजबूर किया। यह 15 जुलाई, 1947 को हुआ, लेकिन सिर्फ छह हफ्तों में ही यह ढह गया क्योंकि पूंजी के पलायन ने ब्रिटेन के भंडार को खत्म कर दिया था। ब्रिटेन ने जल्दी से विनिमय नियंत्रण फिर से लागू कर दिए।
1956 के स्वेज संकट में स्थिति और भी खराब हो गई। जब मिस्र के गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने नहर पर कब्जा करने के लिए मिस्र पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पाउंड और फ्रैंक पर भारी दबाव के कारण उनके विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गए, क्योंकि अमेरिका ने वित्तीय मदद देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह था कि अमेरिका पुराने किस्म के उपनिवेशवाद का विरोधी था। ब्रिटेन और फ्रांस को स्वेज से शर्मनाक वापसी करनी पड़ी और वास्तव में पुराने किस्म के उपनिवेशवाद से भी। वे अमेरिकी मंजूरी के बिना विदेशी सैन्य रोमांच पर नहीं निकल सकते थे।
1958 तक ब्रिटेन के लिए पर्याप्त परिवर्तनीयता संभव हो गई थी। फिर भी, 1976 में, पाउंड पर भारी दबाव के कारण उसे 3.9 बिलियन डॉलर का IMF बेलआउट लेना पड़ा। केवल 1979 में ब्रिटेन इतना मजबूत और आत्मविश्वासी हुआ कि उसने स्टर्लिंग को पूंजी खाते पर पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया। इसमें 30 से अधिक वर्षों की बाधाएं, पूंजी प्रतिबंध और अपमान शामिल थे।
ब्रिटेन सिटी ऑफ लंदन और अपनी स्थापित वित्तीय प्रणाली का घर है। अगर यह देश अस्थिर पूंजी प्रवाह से इतना कमजोर हो सकता है, तो भारत को तो और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पिछले हफ्ते जैसे छोटे-छोटे कदम ठीक हैं। लेकिन इससे कुछ भी ज्यादा महत्वाकांक्षी करने से बचना चाहिए। पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में तो दशकों तक सोचना भी नहीं चाहिए।






